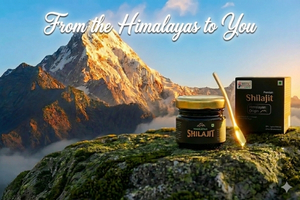भाषा विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है। हम अपनी बात को कभी सीधे - सादे ढंग से कहना चाहते हैं और कभी प्रभावशाली ढंग से। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग उसे प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है।
मुहावरा अर्थात अभ्यासः
अभ्यासवश एक अभिव्यक्ति कभी-कभी एक विशेष अर्थ देने लगती है। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करें, मुहावरा कहलाता है। इसे वाग्धारा भी कहते हैं।
लोकोक्तियां या कहावतें लोक - अनुभव का परिणाम होती हैं। किसी समाज ने लंबे अनुभव से जो कुछ सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया, कुछ कवियों ने, कुछ प्रबुद्ध लोगों ने। उसकी सच्चाई सभी स्वीकार करते हैं। कविताबद्द लोकोक्तियों को सूक्ति भी कहते हैं।
मुहावरे के शब्द अपने कोषगत अर्थों को छोड़कर कुछ भिन्न अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्ति अपने मूल अर्थ से जुड़ी रहती है। इसके अतिरिक्त मुहावरा पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होता है परंतु लोकोक्ति पूर्णतया वाक्य में बंधी होती है। अतः वाक्य के भीतर आते हैं मुहावरा तो वाक्य का अंग बन जाता है परंतु लोकोक्ति एक उपवाक्य के रूप में ही रहती है।
वाक्य - प्रयोग के समय मुहावरे में आए शब्दों के रूप लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण बदलते रहते हैं, लोकोक्ति ज्यों की त्यों रहती हैं।
लोकोक्ति के जो शब्द रहते हैं उसका अर्थ बहुत गुढ़ (गहरा) होता है। अपनी अपनी समझ के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझते हैं।
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
दो अलग-अलग वाक्यों को यहां पर जोड़ा गया हैः-
हाथ कंगन को आरसी क्या - अर्थात हाथ में कंगन पहने हैं, तो उसके लिए आईने की क्या आवश्यकता है, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
पढ़े लिखे को फारसी क्या - अर्थात फारसी भाषा बहुत कठिन होने के कारण हर व्यक्ति इसे नहीं पढ़ सकता। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है।
उदाहरणः इस दवाई को पाँच दिन खाकर देख लीजिए कितना लाभ पहुंचाती है।